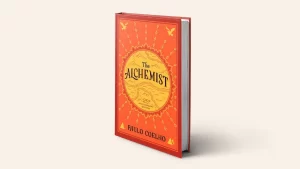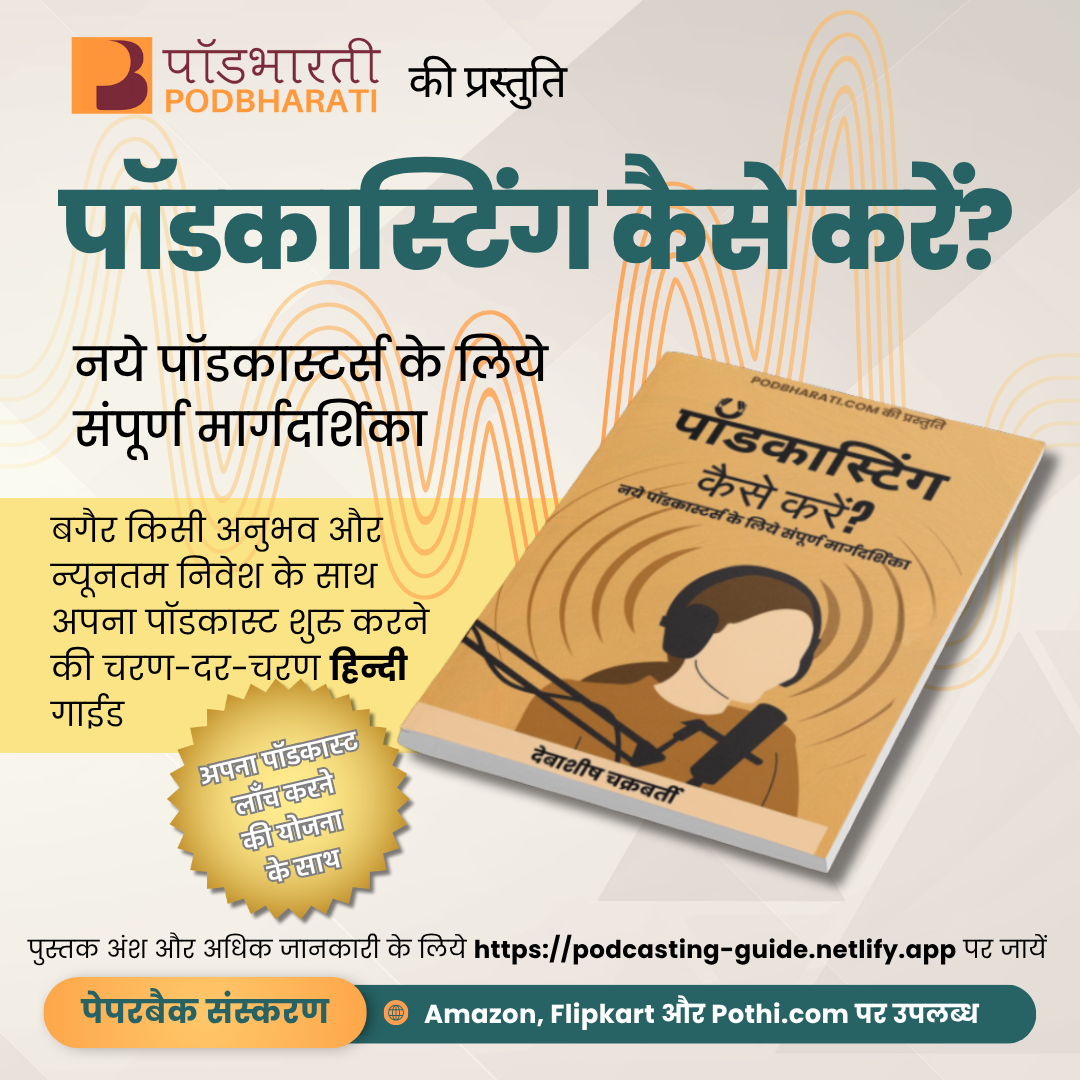आपकी रचनायात्रा में आई.आई.टी कानपुर का खासा योगदान रहा। इस दौरान काफी कष्ट भी उठाने पड़े। क्या परिस्थितियां रहीं?
 देखिये जब मैं आई.आई.टी.गया था तो दो बातें थीं। एक तो मैं हिंदी का आदमी था दूसरे गैर तकनीकी। तो वहां के लोगों ने शुरु में मुझे बिल्कुल सहन नहीं किया। बल्कि विरोध किया और उसके कारण मुझे मुझे तमाम कष्ट उठाने पड़े। एक और बात थी कि मेरा लगाव वहां के छात्रों तथा दूसरी-तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों से ज्यादा था जिसे वहां के ‘टॉप लीडर्स’ या फैकल्टी नापसंद करती थी। मेरे सामने एक बड़ा सवाल था कि ये प्रोफेसर जो विदेशों में रहते हुये अपना सारा काम खुद करते हैं वे यहां चपरासियों को लेकर लड़ाई करते थे। इसी सब को लेकर वहां फैकल्टी से कभी-कभी कहा-सुनी, तनाव हो जाता था। सस्पेन्ड भी हुआ मैं। मुकदमा लड़ना पड़ा। अंततः उच्च न्यायालय में केस जीता और बहाल हुआ। निदेशक तथा चेयरमैन को इस्तीफा देना पड़ा। पर तमाम कष्ट के बावजूद मैंने प्रयास किया कि इंस्टीट्यूट को नुकसान न होने पाये।
देखिये जब मैं आई.आई.टी.गया था तो दो बातें थीं। एक तो मैं हिंदी का आदमी था दूसरे गैर तकनीकी। तो वहां के लोगों ने शुरु में मुझे बिल्कुल सहन नहीं किया। बल्कि विरोध किया और उसके कारण मुझे मुझे तमाम कष्ट उठाने पड़े। एक और बात थी कि मेरा लगाव वहां के छात्रों तथा दूसरी-तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों से ज्यादा था जिसे वहां के ‘टॉप लीडर्स’ या फैकल्टी नापसंद करती थी। मेरे सामने एक बड़ा सवाल था कि ये प्रोफेसर जो विदेशों में रहते हुये अपना सारा काम खुद करते हैं वे यहां चपरासियों को लेकर लड़ाई करते थे। इसी सब को लेकर वहां फैकल्टी से कभी-कभी कहा-सुनी, तनाव हो जाता था। सस्पेन्ड भी हुआ मैं। मुकदमा लड़ना पड़ा। अंततः उच्च न्यायालय में केस जीता और बहाल हुआ। निदेशक तथा चेयरमैन को इस्तीफा देना पड़ा। पर तमाम कष्ट के बावजूद मैंने प्रयास किया कि इंस्टीट्यूट को नुकसान न होने पाये।
वहां हिंदी क्या स्थिति थी उन दिनों? आपके आने पर हालात कुछ बदले?
मेरे आने से पहले वहां हिंदी में कोई बात नहीं करता था। सब जगह अंग्रेजी में बोर्ड लगे थे। मैंने द्विभाषी कराये। लोगों में भी बदलाव आये। वे हिंदी में बात करने लगे। जब मैं बहाल होकर आया तो मैंने उनसे कहा, "देखिये आपको भी मुझसे असुविधा है, मुझे भी आपसे। मैं बस एक रचनात्मक लेखन केन्द्र खोलना चाहता हूं।" इसे उन्होंने सहर्ष मान लिया।
आपके किसी उपन्यास में फैकल्टी द्वारा सताये जाने पर किसी छात्र की आत्महत्या का जिक्र है!
हां, सरकार का एक आदेश आया की एस.सी, एस.टी. छात्रों की भर्ती कोटे से की जाये। तो उनका ‘कट प्वाइंट’ बहुत ‘लो’ कर दिया गया। इसका वहां के अन्य छात्रों व फैकल्टी के लोगों ने बहुत विरोध किया। जिसके कारण इन छात्रों को बहुत कुछ सहना पड़ा। उनकी पढ़ाई में समस्या आयी। उनको हेय दृष्टि से देखा गया। लोग उनका सहयोग नहीं करना चाहते थे। पढ़ाना नहीं चाहते थे उनको। अपमानित कर कक्षा में ताने मारते थे कि आप लोग कहां से आ गये। इससे तंग आकर एक छात्र ने आत्महत्या कर ली। मैंने ‘परिशिष्ट’ उपन्यास में इसका जिक्र किया है।
कई लोगों मानते हैं कि करोड़ों अरबों के आई.आई.टी बनाने से बेहतर होता कि हम अच्छे पॉलीटेक्निक और आई.टी.आई बनायें, ऐसे लोग जो कि सचमुच में इंजीनियेरिंग करते हैं। आप वहां लंबे अर्से रहे हैं। आपकी क्या सोच है इस बारे में?
मैं आपसे सहमत हूं। यह सही है कि आई.आई.टी.से देश को कोई फायदा नहीं है। असल में ये टेक्निकल लेबर के रिक्रूटिंग इंस्टीट्यूट बन गये हैं विकसित देशों के लिये। हम अपने कुशल तकनीकी लेबर उनको सप्लाई करते हैं। ज्यादातर लोग विदेश चले जाते हैं जहां इनको हाथों-हाथ लिया जाता है। जो रह जाते हैं यहां वे बहुराष्टीय कम्पनियों में चले जाते हैं। देश को इनसे बहुत कम फायदा है।
कहा जाता है कि यहां भर्ती ज्यादातर छात्रों का तन तो यहां रहता है पर मन अमेरिका में?
यहां ज्यादातर छात्र मध्यवर्ग से आते हैं। वहां की सुख-सुविधायें आकर्षित करती हैं। यहां भी जो ‘फैकल्टी’ होती है वह ऐसा वातावरण तैयार करती है। पाठ्यक्रम और केस स्टडी वहां के हिसाब से तय होते हैं। अमेरिका से आंकड़े लेकर उसे यहां फीड करके योजनायें बनाई जाती है। जिससे स्वाभाविक रूप से वहां जाने की ललक होती है। एक लड़का था जो विदेश नहीं जाना चाहता था बाद में वहां जाकर इतना रम गया कि वापस आने का नाम नहीं लिया। वह अपने सीनियर्स के लिये रोबोट की तरह हो गया। मैंने अपने उपन्यास "अन्तर्ध्वंस" में इसका जिक्र किया है। इससे भी लोग यहां लोग मुझसे नाराज हुये।
देखा गया है कि परदेश जाने के बाद लोगों के मन में देश के लिये प्यार बढ़ जाता है। काफी आर्थिक सहायता करने लगते है वे देश की।
जब विदेश जाते हैं लोग तो देश की यादें आना,लगाव होना स्वाभाविक होता है। अतीत दूर तक पीछा करता है। एक लड़का विदेश में परिचित प्रोफेसर से मिलने जाता है तो वह पूछता है कि तुम अरहर की दाल लाये हो? उसके पास सहगल,रफी के पुराने गानों के कैसेट हैं। वह कहता है कि जब मैं यहां की जिंदगी से ऊबता हूं तो इन रिकार्ड को सुनने लगता हूं। जो आर्थिक सहायता वाली बात है वो कुछ हद तक सच है। होता यह है कि देश के लिये जो वो पैसा भेजते हैं उनका अधिकतर भाग ‘फंडामेंटलिस्ट’ के पास पहुंच जाता है। वे तो समझते कि वे देश की मदद कर रहे हैं लेकिन चक्र कुछ ऐसा बनता है कि उनका पैसा देश की मदद में न लगकर देश को बांटने में लग जाता है।
पहला गिरमिटिया लिखने के पहले और गांधी के बारे में आठ साल शोध करके इसे लिखने के बाद आपने अपने में कितना अन्तर महसूस किया?
देखिये मैं आपको एक बात सच बताऊं कि अगर मैं आई.आई.टी.न गया होता तो शायद पहला गिरमिटिया न लिख पाता। वहां मैंने जिस अपमान व कठिनाइयों का सामना किया तो कहीं न कहीं मुझे गांधीजी ने दक्षिण अफ्रीका में जो अनुभव किये होंगे। हालांकि न मेरी गांधी से कोई बराबरी है न मैं वैसी स्थिति में हूं पर उनके बारे में सोचने की मेरी मानसिकता अवश्य बनी। मुझे लगा कि हमें इस बात को समझना चाहिये कि ऐसी कौन सी शक्ति थी जिसने इस आदमी को महात्मा गांधी बनाया। एक आम, डरपोक किस्म का आदमी जो बहुत अच्छा बोलने वाला भी नहीं था। वकालत में भी असफल। इतना फैशनेबल आदमी। वह इतना त्यागी और देश के लिये काम करने वाला बना। मुझे हमेशा लगता रहा कि जरूर उसने अपने तिरस्कार से ऊर्जा ग्रहण की जिसके कारण वह अपने को इतना काबिल बना पाया। इससे मुझे भी अपने को प्रेरित करने की जरूरत महसूस हुई।
दक्षिण अफ्रीका में लोग गांधी को किस रूप में देखते हैं?
मैंने पहले भारत के गांधी के बारे में लिखना शुरु किया था। जब मैं दक्षिण अफ्रीका गया तो वहां हासिम सादात नाम के एक सज्जन ने मुझसे कहा, "देखिये गांधी हमारे यहां तो जैसे खान से निकले अनगढ़ हीरे की तरह आया था जिसे हमने तराशकर आपको दिया। आपको तो हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिये। अगर आपको लिखना है तो इस गांधी पर लिखिये।" उनकी बात ने मुझे अपील किया तथा मैंने उस पर लिखा।
जब यह प्रकाशित हुआ था तो कुछ लोगों मसलन राजेन्द्र यादव ने इसका भारी-भरकम होना ही एक विशेषता बतायी थी।
इसका एक कारण है कि हिंदुस्तान में एक वर्ग है जो गांधी को पसन्द नहीं करता। उनको लगता है कि गांधी के वर्चस्व से लेफ्टिस्ट मूवमेंट पर असर पड़ेगा। हालांकि वामपंथियों ने भी इसे बहुत सराहा। नामवर सिंह ने सराहना की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े विष्णुकान्त शास्त्रीजी ने बहुत तारीफ की। हर एक की सोच अलग होती है। हर एक को अपनी धारणा बनाने का अधिकार है।
लोग कहते हैं गांधीजी अपने लोगों के लिये डिक्टेटर की तरह थे। अपनी बात मनवा के रहते थे। आपने क्या पाया ?
वो तो देखिये जब आदमी कुछ सिद्धान्त बना लेता है तो उनका पालन करना चाहता है। जैसे किसी ने त्याग को आदर्श बनाया तो उपभोग की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना चाहता है। गांधीजी तानाशाह नहीं थे। हां उनके तरीके अलग थे। एक घटना बताता हूं। गांधी एक बार इटली के तानाशाह मुसोलिनी से मिलने गये। साथ में उनके सचिव महादेवदेसाई तथा मीराबेन और मुसोलिनी का एक जनरल था जिससे मुसोलिनी नाराज था। गांधीजी उसी जनरल के घर रुके थे। मुसोलिनी ने गांधी का स्वागत किया और एक कमरे में गये सब लोग जहां केवल दो कुर्सियां थीं। मुसोलिनी ने गांधी को बैठने को कहा। गांधी ने तीनों को बैठने को कहा। तो ये कैसे बैठें? मुसोलिनी ने फिर गांधी को बैठने को कहा। गांधी ने फिर तीनों से बैठने को कहा। तीन बार ऐसा हुआ। आखिरकार तीन कुर्सियां और मंगानी पड़ीं। तब सब लोग बैठे। तो यह गांधी का विरोध का तरीका था। कुछ लोग इसे डिक्टेटरशिप कह सकते हैं।
इसी तरह दूसरे विश्वयुद्ध में उन्होनें हिटलर को लिखा था, "यू आर रेस्पान्सिबल फार द वार एन्ड यू हैव टु वाइन्ड इट अप"। मैंने इस पर हिटलर का जवाब भी देखा। उसने लिखा था, "नो दीज़ प्यूपल आर ब्लेमिंग मी अननेसेसरली, एक्चुअली दे आर रेस्पान्सिबल फार द वार, एन्ड यू मस्ट टाक टू देम।"
मीरा बेन के बारे में सुधीर कक्कड़ ने लिखा है कि वे गांधीजी को चाहती थीं। गांधीजी के मन में भी उनके लिये कोमल भाव थे। सचाई क्या थी?
इस तरह से अनर्गल बातें लिखने का कोई आधार नहीं है। मीरा बेन लंदन से गांधी के लिये तो ही आयीं थीं। गांधी को समर्पित होकर। वे उनके प्रति आसक्त भी थीं। ब्रिटेन की संस्कृति के हिसाब से इसमें कुछ अटपटा नहीं था। पर गांधी ने कई बार उनको अपने से दूर रखा। समझाते रहे। पत्र लिखते रहे कि मेरे पास आने के बजाय तुम काम करो। सेवा करो। इससे तुम्हें शान्ति मिलेगी।
आपकी कौन सी कृति ऐसी है जिसे आप जैसा चाहते थे वैसा लिख पाये?
ऐसा कभी नहीं हुआ। रचनात्मकता में ऐसा होता है कि आदमी जो करना चाहता वह नहीं कर पाता। और चीजें जुड़ती जाती हैं। मानव मस्तिष्क कुछ इस तरह है कि जब आप कुछ करना शुरु करते हैं तो काम शुरु करने पर नई-नई संभावनायें नजर आने लगती हैं। वह उस रास्ते चल देता है। पुरानी चीजें छूट जाती हैं। नयी दिशायें खुलती हैं। जब मैंने गांधी पर लिखना शुरु किया तो भारत के गांधी मेरे सामने थे। जब दक्षिण अफ्रीका गया तो पाया कि असली गांधी तो यहां हैं – मैं उस तरफ चल पड़ा। यह रचनात्मकता की एक सीमा भी है और उसका विस्तार भी।
कानपुर के वर्तमान साहित्यिक परिवेश के बारे में क्या विचार हैं आप के?
पहले यहां साहित्यिक नर्सरी थी। रमानाथ अवस्थी, नीरज, उपेन्द्र जैसे गीतकार यहां हुये । प्रतापनारायण मिश्र , विशंभरनाथ शर्मा ‘कौशिक’ सरीखे गद्य लेखक थे। प्रेमचंद थे। अब छुटपुट लोग हैं। वे भी कितना कर पाते हैं। उनकी भी सीमायें हैं।
कानपुर कभी भारत का मैनचेस्टर कहलाता था। आज मिलें बंद हो गयीं। कानपुर किसी उजड़े दयार सा लगता है। क्या ट्रेड यूनियनों के ईंट से ईंट बजा देने के जज्बे की भी इस हालत तक पहुंचने के लिये जिम्मेदारी है?
मेरी व्यक्तिगत राय यह है कि विदेशों में जो मार्क्सवादी गतिविधियां हुयीं उसमें उन्होंने उत्पादन नहीं प्रभावित होने दिया। विरोध किया पर उत्पादन चलता रहा। हमारे यहां उत्पादन सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। आप अधिकार मांगिये, सब बातें करिये पर उत्पादन, जो मांगों का मूल आधार है, उसे ठप्प कर देंगे, फैक्ट्री बंद कर देंगे तो बचेगा क्या? लड़ेंगे किसके लिये?
सन् 67 में जब मैं यहां आया था तो ये सब फैक्ट्रियां चलतीं थीं। शाम को यहां सड़क पर घण्टे भर लोगों के सर ही सर नजर आते थे। दुकानें थीं। बहुत से लोग बैठते थे। सामान बेचते थे। लोग उधार ले जाते । तन्ख्वाह मिलने पर पैसा चुका देते। लेकिन मिलों के बंद होने से सब बेरोजगार हो गये। पहले जब कोई मरता था तो उसके बच्चे को रोजगार मिल जाता था। अब खुद की नौकरी गयी,बच्चे का भी आधार गया। जो दुकानदार अपनी बिक्री के लिये इन पर निर्भर थे वे भी उजड़ गये। इस बदहाली के मूल में कहीं न कहीं आधार की अनदेखी करना कारण रहा।
आज दुनिया में अमेरिकी वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। अपनी पिछली चीन यात्रा में आपने वहां क्या बदलाव देखे?
मैं पिछले साल अक्टूबर में चीन गया था। वहां देखा कि चीन एकदम अमेरिका हो गया है। चीनी महिलायें अपनी पारम्परिक पोशाक छोड़कर अमेरिकन शार्टस, स्कर्ट में दिखीं। मेरे ख्याल में महिलायें ज्यादा आजाद हुयीं हैं वहां आदमियों के मुकाबले।
जब आपने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला होते देखा टीवी पर, तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी?
हालांकि मैं हिंसा का हिमायती नहीं हूं पर मैंने इस बारे में ‘अकार’ के संपादकीय में लिखा था, "ऐसा लगा जैसे किसी साम्राज्ञी को भरी सभा में निर्वस्त्र कर दिया गया हो। सारे देशों के महानायक उसे शर्मसार होने से बचाने के लिये समर्थनों की वस्त्रांजलियां लेकर दौड़ पड़े हों।" उसके बाद हमें यह भी दिखा कि कितने डरपोंक हैं अमेरिकन। मरने से कितना डरते हैं वे। मुझे लगता है कि अगर एकाध बम वहां गिर जाते तो आधे लोग तो डर से मर जाते वे। पाउडर के डर से हफ्तों कारोबार ठप्प रहा वहां।
हंस में जो "मेरे विश्वासघात" के नाम से लोगों में अपने यौन विचलनों को खुल के लिखने की शुरुआत हुयी इसको आप किस तरह देखते हैं?
यह तो उकसावे का लेखन है। पानी पर चढ़ाकर लिखवाना। राजेन्द्र यादव ने देह वर्जनाओं से मुक्ति के नाम पर लिखने को उकसाया। बाद में रामशरण जोशी ने कहा भी कि इसे मत छापो पर राजेन्द्र यादव ने छाप दिया। इसी के कारण उसकी नौकरी भी चली गयी। दरअसल एक संपादक का यह भी दायित्व होता है कि वह देखे कि जो वह छापने जा रहा है उससे लेखक का कोई नुकसान तो नहीं हो रहा। राजेन्द्र यादव ने यह नहीं देखा। भुगतना पड़ा लेखक को।
आज देश की हालत को आप किस रूप में पाते हैं?भविष्य कैसा सोचते हैं आप इसका?
आज देश की राजनैतिक हालत बहुत खराब है। नेताओं में कोई ऐसा नहीं है जो आदर्श प्रस्तुत कर सके। अटल जैसे नेता तक रोज अपने बयान बदलते हैं। ऐसे में निकट भविष्य में किसी बड़े बदलाव के आसार तो मैं नहीं देखता। आगे यह हो सकता है कि युवा पीढ़ी अपने आदर्श खुद तय करे। ग्लोबलाइजेशन का यह फायदा हो सकता है कि लोगों में आगे बढ़ने की प्रवृत्ति बढ़े तथा वह आर्थिक समानता के लिये प्रयास करे और विकास की गति तय हो।
आपकी पसंदीदा पुस्तकें कौन सी हैं?
मुझे नरेश मेहता की "यह पथ बंधु था", यशपाल का "झूठा सच", अज्ञेय की "शेखर एक जीवनी" काफी पसंद हैं। अभी मैं पाकिस्तान गया था तो वहां "झूठा सच" बहुत याद आया।
पसंदीदा व्यंग्य लेखक कौन हैं आपके?
शरद जोशी मुझे बहुत अच्छे लगते रहे। आजकल ज्ञान चतुर्वेदी बढ़िया लिख रहे हैं।
निरंतर के पाठकों के लिये कोई संदेश देना चाहेंगे?
मुझे तो आप लोगों का यह प्रयास बहुत अच्छा लगा। जिस तरह अलग-अलग देशों रहने वाले आप भारतीय लोग हिंदी के प्रसार के लिये प्रयत्नशील हैं वह सराहनीय है। मेरे ख्याल में इसकी इस समय जबरदस्त जरूरत है। इससे विज्ञान की भाषा बनने में भी बहुत मदद मिलेगी। आगे चलकर यह बहुत काम आयेगा। जिस तरह आज अखबार रीजनल, लोकल होते जा रहे हैं, उनका दायरा सिमटता जा रहा है। ऐसे समय में नेट के माध्यम से दुनिया तक पहुंचने के प्रयास बहुत जरूरी हैं। आप सभी को मैं इस सार्थक काम में लगने के लिये बधाई देता हूं तथा सफलता की मंगलकामना करता हूं।